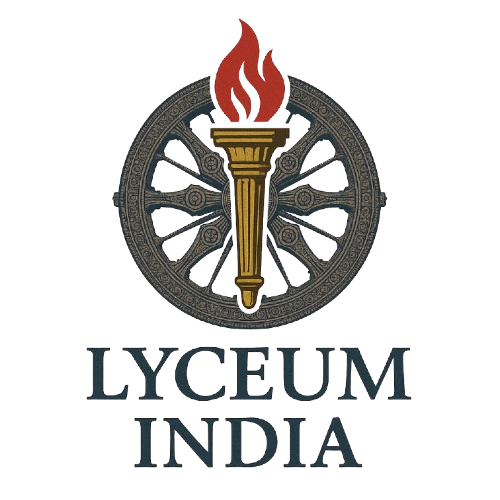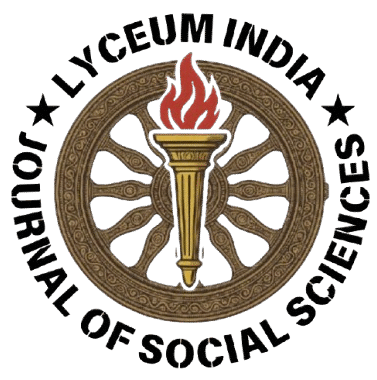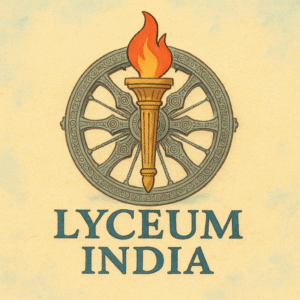Lyceum India Journal of Social Sciences ISSN: 3048-6513 (Online)
Volume: 2 Issue: 4 (SEPTEMBER 2025)
| Title: | Beyond Survival: The Enduring Agony and Emerging Rights of Transgender Individuals | |
| Author(s) | Dr. Madhu Thawani | |
| Pages | 1-8 | DOI: 10.5281/zenodo.17222447 |
| Abstract: | This article undertakes an exhaustive exploration of the profound and often agonizing experiences faced by transgender individuals worldwide, with a particular focus on the unique challenges and evolving legal landscape in India. It delves into the intense psychological distress of gender dysphoria, the pervasive societal burden of discrimination and prejudice, and the arduous journey toward self-acceptance and affirmation. Drawing upon global research and highlighting India’s legal advancements, this paper meticulously examines systemic obstacles, including inadequate healthcare access, legal hurdles in identity recognition, familial rejection, and social ostracization, which collectively contribute to significant mental health disparities. Crucially, it elaborates on the landmark judgments and legislative frameworks, such as India’s NALSA v. Union of India (2014) judgment and the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, while also discussing their limitations and the ongoing challenges in effective implementation. Understanding these profound and often unseen struggles, alongside the crucial role of legal protections, is vital for fostering empathy, advocating for truly inclusive policies, and creating supportive environments that affirm the identities and well-being of transgender individuals. | |
| Keywords: | Transgender, Gender Dysphoria, Discrimination, Transgender Persons (Protection of Rights) Act, NALSA judgment, Human Rights, Legal Recognition. | |
| Certificate | ||
| Title: | Christianity and Power/Knowledge: Understanding Foucault’s Theorisation of Religious Practices | |
| Author(s) | Brajesh Kumar | |
| Pages | 9-17 | DOI: 10.5281/zenodo.17222475 |
| Abstract: | Michel Foucault has theorized Christianity as a discourse that combines truth and power with the development of the subjective knowledge of the self. It claims that Christianity was a historical mechanism of the production of truth about self and the modification of self through practices like confession, penitential rites, and monastic obedience. This ritual process, in turn, serves to consolidate institutional authority. Using Foucault’s archaeological and genealogical methods, the paper delves into the emergence of the categories of truth, like sin/purity and temptation/obedience. These truth categories then guide individuals’ behaviour and force them to surrender before the Christian discourses. Foucault’s theorisation has been criticised for being Eurocentric and reductionist. However, he described how religious practice is immersed in regimes of power/knowledge. This paper argues that Christianity should not be read as simply a belief system but as a discursive formation. | |
| Keywords: | Christianity, Confession, Michel Foucault, Power/Knowledge, and Subjectivity | |
| Certificate | ||
| Title: | Electoral Reform and Civil Society in Mizoram: Assessing the Impact and Limitations of the Mizoram People’s Forum (MPF) | |
| Author(s) | Fiona Lalmalsawmi & Dr. H. Lalzuithangi | |
| Pages | 18-27 | DOI: 10.5281/zenodo.17222485 |
| Abstract: | This paper explores the role and influence of the Mizoram People’s Forum (MPF), a distinctive church-backed civil society organization, on the electoral process in Mizoram. Established in 2006 by the state’s major churches, the MPF has emerged as a crucial force dedicated to combatting electoral malpractices and fostering free, fair and peaceful elections. This study posits that the MNF has fundamentally reshaped Mizoram’s political landscape by leveraging its moral and social authority to cultivate a culture of ‘clean politics’. Through its key strategies – including formalizing a code of conduct with political parties, limiting campaign expenditures, and implementing comprehensive voter education programs, the MPF has significantly diminished the power of money in politics and promoted a more transparent and accountable political environment. This research highlights that the MPF’s success is rooted in its extensive civil society network and the high level of public trust it enjoys. While recognizing certain limitations, the paper highlights that the MPF has established a unique and effective model for democratic reform, positioning Mizoram as an exemplary case of civil society serving as a powerful catalyst for electoral integrity. | |
| Keywords: | Mizoram People’s Forum, church, civil society, electoral reform, clean politics | |
| Certificate | ||
| Title: | Emergence of Sixth Schedule in the Constitution of India | |
| Author(s) | Lalbiakzami Ralte & Prof. Jangkhongam Doungel | |
| Pages | 28-35 | DOI: 10.5281/zenodo.17222518 |
| Abstract: | This paper examines the colonial policies that were enforced in the areas now governed under the Sixth Schedule prior to India’s independence. It will discuss in detail how these policies shaped the administration and socio-political conditions of tribal regions, laying the groundwork for later constitutional safeguards. Further, the paper will analyse the steps undertaken by the Constituent Assembly in addressing the unique concerns of tribal communities, which eventually culminated in the framing of the Sixth Schedule of the Indian Constitution. Attention will also be given to the debates within the Constituent Assembly, highlighting the discussions, disagreements, and consensus-building that influenced the decision to provide a special constitutional framework for tribal areas. | |
| Keywords: | Sixth Schedule, Constituent Assembly, Constitution, Committee, Government | |
| Certificate | ||
| Title: | Green Economy in India: prospects and Difficulties | |
| Author(s) | Tribikram Sunani | |
| Pages | 36-41 | DOI: 10.5281/zenodo.17222572 |
| Abstract: | The economic development of India has been growing rapidly since the introduction of economic reforms in 1991. Despite the economic growth, the economic reforms have brought along with them the significant increase of the pollution, resource depletion and climate change. Though economic development is essential, it must not be at the expense of environmental degradation, which is the real-time demand. This paper explores the relationship between economic development and environmental crisis by emphasising the need for green economic transformation. The study finds that rapid economic development has contributed significantly to environmental degradation. This paper concludes with the note that in order to fully integrate green economy principles along with the economic development process, substantial efforts to combine and apply are necessary. | |
| Keywords: | Green Economy, Economic Development, Environment, Pollution | |
| Certificate | ||
| Title: | Livelihood Diversification and Challenges: A Case Study of Mao Tribe of Senapati District of Manipur | |
| Author(s) | Dr. B Komow & Dr. Bimla Rai | |
| Pages | 42-48 | DOI: 10.5281/zenodo.17222620 |
| Abstract: | The Mao tribe in Manipur is dependent on agriculture for their livelihood. Traditionally, they practiced dry and wet terrace cultivation which is mainly for self-consumption. The Mao inhabited area has a high potential for high-value crops due to moderate climate and fertile soil. The National Highway -2 (NH-2) which passes through Mao area has been a significant factor for livelihood diversification and commercialization of agriculture crops. They have shifted from subsistence paddy cultivation to horticulture for commercial purposes as an alternative to income generating source and livelihood opportunity. Thus, the paper examines the changing pattern of livelihood of the Mao tribe, with focus on the factors influencing diversification and the related challenges. | |
| Keywords: | Mao Tribe, Livelihood, Horticulture, Floriculture, Livelihood Strategies | |
| Certificate | ||
| Title: | Reminiscing the Asian Games 1998 and Boxer Dingko Singh | |
| Author(s) | Tenzing Singh Ngasham | |
| Pages | 49-53 | DOI: 10.5281/zenodo.17222632 |
| Abstract: | This research article reflects the 1998 Asian Games in Bangkok and the impact of Dingko Singh as an Indian boxer. His splendid achievement in winning gold in the boxing arena epitomises a pioneer spirit, unrelenting focus, and pride of the nation. Rise from humble beginnings in Manipur, India, which has an underdeveloped sports arena and minimal support for aspiring sportspeople. Towards the end of his life, he bravely battled liver cancer and COVID-19. In conclusion, the article mentions that Dingko Singh earned the title of a national hero and is credited with inspiring a generation of young Indian boxers, especially Mary Kom, Laishram Sarita Devi, Devendro Singh, and many more. | |
| Keywords: | Dingko Singh, 1998 Asian Games, Boxing, India | |
| Certificate | ||
| Title: | State And Market Dynamics: Challenges and Opportunities in Contemporary India | |
| Author(s) | Dr. Ravichandra Walikar & Sri. Guranna Venkanagouda Raraddi | |
| Pages | 54-60 | DOI: 10.5281/zenodo.17222673 |
| Abstract: | The relationship between the State and the Market has always been a decisive factor in shaping the trajectory of India’s socio-economic development. In contemporary times, this dynamic has acquired greater complexity due to the forces of globalization, liberalization, technological transformation, and socio-political change. On the one hand, the market has emerged as a powerful driver of innovation, efficiency, and wealth creation; while on the other hand, the State continues to play an indispensable role in ensuring equity, regulation, social justice, and long-term stability. This article critically examines the interdependence of State and Market in India, highlighting both challenges and opportunities. Among the key challenges are economic inequality, regional disparities, market monopolization, regulatory gaps, corruption, and the tension between public welfare and private profit. At the same time, opportunities arise in the form of public–private partnerships, digital governance, inclusive growth models, welfare-oriented policies, and sustainable development strategies. The paper also explores how India’s federal structure, democratic institutions, and developmental priorities influence the balance between State intervention and market freedom. By analysing contemporary policy debates such as privatization vs. state control, welfare distribution vs. fiscal prudence, and globalization vs. protectionism the study underscores the need for a synergistic approach where the State and Market complement rather than conflict with each other. | |
| Keywords: | State, Market, India, Globalization, Development, Governance, Inequality, Public Policy | |
| Certificate | ||
| Title: | Strengthening Ethnic Diversity: Empowering Ethnic Heritage of the Deori community of Assam within the Vision of Viksit Bharat | |
| Author(s) | Dr. Dilip Kumar Sonowal | |
| Pages | 61-69 | DOI: 10.5281/zenodo.17222704 |
| Abstract: | The distinctive customs and strong ethnic heritage of the Deori people have heavily contributed to the ethnic richness of India. Their rites, rituals, oral traditions, and festivals, as well as their socio-cultural norms such as unique dress, village structure, marriage and family system, position of women, food habits, and traditional music and dance, reinforce their ethnic identity. These customs contribute enormously to the transmission of values, ethics, and morals to subsequent generations. The natural environment also mirrors centuries-old traditional wisdom and cultural ownership of the Deoris. By safeguarding and strengthening this heritage, India can retain its cultural diversity while promoting the national vision of a developed and prosperous nation. This paper examines the Deori cultural heritage of Assam and how empowering it will be a source of strength to India’s ethnic diversity in realizing Viksit Bharat’s vision. | |
| Keywords: | Deori Community, Ethnic Heritage, Ethnic Diversity, Socio-Cultural Norms, Viksit Bharat | |
| Certificate | ||
| Title: | Tribal Welfare in India: Policy Frameworks, Implementation Challenges, and Future Prospects | |
| Author(s) | Manjunath Pujar | |
| Pages | 70-82 | DOI: 10.5281/zenodo.17222727 |
| Abstract: | This research article critically examines the policy frameworks governing tribal welfare in India, evaluates the challenges in their implementation, and explores future prospects for inclusive development. Despite constitutional safeguards and targeted schemes like the Forest Rights Act (FRA), Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA), and Tribal Sub-Plan (TSP), India’s tribal communities continue to face systemic marginalization, underdevelopment, and socio-economic exclusion. The study highlights persistent issues such as inadequate policy execution, bureaucratic inefficiencies, resource diversion, and lack of community participation. By analysing central and state-level initiatives, the paper underscores the gaps between policy intent and ground-level realities. It also emphasizes the need for culturally sensitive governance, decentralized planning, and greater accountability mechanisms. The article concludes with actionable recommendations for strengthening tribal welfare through participatory governance, effective monitoring, and sustainable development practices. This study contributes to the discourse on tribal empowerment and policy reforms essential for achieving equitable growth in India’s diverse socio-cultural landscape. | |
| Keywords: | Tribal Welfare, Policy Implementation, Scheduled Tribes, Forest Rights Act (FRA), Inclusive Development, Governance Challenges | |
| Certificate | ||
| Title: | Windows to Resilience: Afghan Women’s Voices and Cultural Reflections in Nadia Hashimi’s A House Without Windows | |
| Author(s) | Kanchan | |
| Pages | 83-89 | DOI: 10.5281/zenodo.17222755 |
| Abstract: | Nadia Hashimi’s A House Without Windows vividly depicts the complex reality of Afghanistan and its people, exploring themes of identity, culture, and resilience within the framework of English literature. The novel reflects Afghanistan’s fraught identity as an Islamic nation grappling with political instability, social upheaval, and cultural intersections. These realities are brought to life through the experiences of Afghan women, whose vulnerability and suffering underscore the profound impact of war and societal unrest. The female characters navigate a world dominated by patriarchal norms, which have long silenced their voices and stifled their aspirations.
The protagonist’s journey from the constraints of a traditional marriage to the unlikely refuge of prison—illuminates the oppressive structures women endure, even within their own homes. The irony of finding solace in incarceration reveals the stark realities of domestic life for many women. Hashimi’s narrative resonates with broader cultural discussions about female oppression and resilience, drawing meaningful connections to other texts that similarly explore struggles for justice and freedom. |
|
| Keywords: | Forced subordination, Patriarchal norms, Vulnerability, Silenced voices, Irony, Societal Constructs, Popular Culture | |
| Certificate | ||
| Title: | Women’s Participation in Local Governance among the Zeme Naga tribe in Nagaland: Problems and Prospects | |
| Author(s) | Dr. P.G.J. Richard & Ms. Idausile Endi | |
| Pages | 90-97 | DOI: 10.5281/zenodo.17222779 |
| Abstract: | The Zeme Naga women continue to face significant barriers in their participation in local governance. It is largely due to the cultural norms backed by patriarchal customary laws. They prioritise men for leadership roles, and these societal expectations often restrict women to family responsibilities rather than encouraging their involvement in governance. This article will explore the role of traditional institutions alongside modern Local governance and highlight women’s participation in local governance. It will also highlight the challenges that the Zeme Naga women faced in participation in local governance. The article concludes by highlighting the amicable strategies for women’s empowerment within the structure of local governance. | |
| Keywords: | Zeme women, Zeme tribe, local governance, traditional institutions, customary laws | |
| Certificate | ||
| Title: | बौद्ध धर्म में राजनीतिक विचार | |
| Author(s) | डॉ. रायन त्र्यंबकराव महाजन | |
| Pages | 98-101 | DOI: 10.5281/zenodo.17222803 |
| Abstract: | प्राचीन काल से ही भारत को वैश्विक स्तर पर एक महान सभ्यता माना जाता रहा है। भारत में अनेक संस्कृतियों और धर्मों के लोग रहते हैं। भारत ने इतिहास, संस्कृति और दर्शन के आधार पर वैचारिक स्तर पर विश्व में अपना स्थान बनाए रखा है। भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचार वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में मिलते हैं। जब जैन धर्म का प्रचार-प्रसार हो रहा था, तब बुद्ध ने एक धर्म दिया, जो आज तक विश्व में विद्यमान है। प्रत्येक धर्म का अपना दर्शन होता है। इसी प्रकार, बौद्ध धर्म का एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और दार्शनिक दर्शन है। बुद्ध ने सद्गुणों और नैतिक आचरण के साथ जीवन जीने पर बल दिया। बौद्ध धर्म एक नैतिक व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य वैदिक धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। बौद्ध धर्म सर्वाधिक सफल रहा क्योंकि यह पूर्व-वैदिक और अवैदिक तपस्वी परंपरा का एक अंग है। यह व्यवस्थित और स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। जिस समय बुद्ध ने अपने विचारों का प्रसार किया, उस समय उन्होंने तीन बातों पर बल दिया, अर्थात् बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध राजनीतिक विचारकों के अनुसार, एक राज्यविहीन और अराजक समाज सभी के लिए खतरनाक है। ऐसी स्थिति में, यदि राजा धर्म और नैतिकता का पालन करे, तो राजतंत्र प्रजा को सुख प्रदान कर सकता है। राज्य के उद्भव के संबंध में अनेक विचारधाराएँ हैं। हालाँकि, बुद्ध के अनुसार, उनका मानना है कि राज्य का निर्माण सामाजिक अनुबंध के माध्यम से हुआ था। भारत में, ऐतिहासिक अहिंसा के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग बुद्ध के दर्शन में हुआ, जब उपनिषदों के लेखकों ने वैदिक यज्ञों की क्रूरता के बारे में बताया। यहीं से शाकाहार के सिद्धांत का विकास हुआ। पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बुद्ध ने अपनी मुख्य शिक्षाओं की वकालत और उन पर ज़ोर दिया, उन्हें समाहित किया, एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया और उन्हें अतुलनीय बनाया। धर्म और शांति के प्रतीक (धर्मचक्र) बौद्ध धर्म ने अहिंसा के क्षेत्र में एक मौलिक योगदान दिया। प्रस्तुत शोध निबंध बौद्ध काल के राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डाल रहा है। | |
| Keywords: | बौद्ध धर्म, राजनीतिक विचार | |
| Certificate | ||
| Title: | भारतीय लोक साहित्य व धार्मिक साहित्यों में निषादों का वर्णन | |
| Author(s) | डॉ. अभिषेक त्रिपाठी & दिनेश चन्द्र | |
| Pages | 102-106 | DOI: 10.5281/zenodo.17222832 |
| Abstract: | भारतीय सामाजिक संरचना का निर्माण मूलतः ग्रामीण एवं शहरी समुदायों में निवास करने वाली हजारों जातियों एवं उपजातियों से हुआ है। विभिन्न धार्मिक समूह या सम्प्रदाय (पन्थ) इन्ही जातियों के बीच क्रीड़ा करते हुए दिखाई देते है। यही कारण है कि भारतीय समाज को अक्सर “एक जातिगत समाज” कहकर परिभाषित कर दिया जाता है। यहां के लोगो की मूल पहचान जाति की रही है। वे पहले अपनी जाति के होते हैं और बाद में बौद्ध, जैन,सिक्ख, वैष्णव अथवा हिन्दू के रूप में उनकी पहचान बनती है। यहां मुसलमान और इसाई भी धार्मिक समूह के अर्थ में कम, जाति के अर्थ में अधिक पहचाने जाते है। भारत में जब विश्व की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद की कविताओं (ऋचाओं) में जाति के संकेत मिलते है। वहां पर जाति के लिए ’ज्ञाति’ तथा ’सजात’ जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। वेदों में कर्मकार (लोहार), नापित (नाई), कूर्मि (कृषक), निषाद (मल्लाह), चर्मकार जैसी जातियों का उल्लेख हुआ है। ब्राहम्ण ग्रन्थ और धर्मसूत्र तो जैसे जातीय निषेधों एवं अधिकारों की सीमा रेखा खींचते हुए दिखायी देते हैं। रामायण, महाभारत तथा अन्य इतिहास ग्रन्थों में जाति व्यवस्था तथा उसके अधिकार एवं कर्तव्यों के साथ ही निषेधों का स्पष्ट क्रियात्मक रूप देखने को मिलता है। स्मृति ग्रन्थ तो जैसे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की रक्षा के लिये विधि विधान अथवा संविधान के रूप थे। जैन तथा बौद्ध धर्म एवं चार्वाक दर्शन का उदय ही ब्राहम्णवादी जातीय तथा धार्मिक व्यवस्थाओं के विरूद्ध एक क्रान्तिकारी आन्दोलन के रूप में हुआ था। चाणक्य द्वारा अर्थशास्थ की रचना में जाति का विचार किया गया है। पुराण सहित अन्य अनेक प्राचीन धार्मिक साहित्य में जाति एवं वर्ण के अधिकार तथा निषेधों की व्यवस्था एवं उनके सुरक्षा की योजना दिखाई देती है, जहां राजा के महत्वपूर्ण कार्यों में जाति एवं वर्ण की रक्षा करना उनका प्रमुख कार्य था। | |
| Keywords: | बौद्ध, जैन, सिक्ख, वैष्णव कर्मकार (लोहार), नापित (नाई), कूर्मि (कृषक), निषाद (मल्लाह), चर्मकार | |
| Certificate | ||
| Title: | संसदीय शासन प्रणाली का ब्रिटेन व भारतीय परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन | |
| Author(s) | डॉ. आरती मिश्रा बलोनी & डॉ. खेमराज चंद्राकर | |
| Pages | 107-113 | DOI: 10.5281/zenodo.17222879 |
| Abstract: | आज की दुनिया में, संसदीय शासन प्रणाली कई नए आयामों का सामना कर रही है। इनमें से कुछ बदलाव वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और सामाजिक मूल्यों में बदलाव जैसे व्यापक रुझानों से प्रेरित हैं, जबकि अन्य विशिष्ट देशों या क्षेत्रों के लिए अद्वितीय हैं। ब्रिटेन और भारत में संसदीय शासन प्रणाली समान सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। इन अंतरों को समझना दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान कर सकता है। संसदीय शासन प्रणाली एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका (सरकार) विधायिका (संसद) के प्रति जवाबदेह होती है। यह प्रणाली दुनिया भर के कई देशों में अपनाई जाती है, जिनमें ब्रिटेन और भारत भी शामिल हैं। हालांकि, दोनों देशों में संसदीय शासन प्रणाली कुछ महत्वपूर्ण अंतरों के साथ लागू की जाती है। | |
| Keywords: | संसदीय प्रजातंत्र, लोकतंत्र, राजशाही, गणतंत्र, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, द्विसदनीय, एकात्मक, संघीय, राजनीतिक दल, चुनाव प्रणाली, प्रथम-पास्ट-द-पोस्ट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, संसदीय सर्वाेच्चता, न्यायिक समीक्षा, जवाबदेही, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्थिरता | |
| Certificate | ||
| Title: | समकालीन भारत में लैंगिक असमानता: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन | |
| Author(s) | ममता मीणा | |
| Pages | 114-119 | DOI: 10.5281/zenodo.17222922 |
| Abstract: | लैंगिक समानता भारतीय संविधान के मूल्यों तथा सतत विकास लक्ष्यों ;ैक्ळेद्ध की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक हैए किन्तु समकालीन भारत में लैंगिक असमानता अब भी विभिन्न रूपों में विद्यमान है। यह शोध पत्र विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से शिक्षाए स्वास्थ्यए रोजगारए राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक.सांस्कृतिक संरचनाओं में मौजूद लैंगिक असमानताओं का अध्ययन करता है। द्वितीयक स्रोतों जैसे जनगणना रिपोर्टए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ;छथ्भ्ैद्धए सतत विकास रिपोर्ट तथा नीतिगत दस्तावेज़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रगति के बावजूद महिलाएँ आज भी निर्णय.निर्माण प्रक्रियाओंए वेतन संरचना और कार्यस्थल पर समान अवसर से वंचित हैं।
संवैधानिक स्तर पर अनुच्छेद 14 ;समानता का अधिकारद्धए अनुच्छेद 15 ;भेदभाव का निषेधद्धए अनुच्छेद 16 ;सार्वजनिक रोजगार में समान अवसरद्धए अनुच्छेद 39 ;राज्य के नीति निदेशक तत्वों में पुरुषों व महिलाओं के लिए समान अधिकारद्ध तथा अनुच्छेद 42 ;मातृत्व संरक्षणद्ध महिलाओं को महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। वहींए सरकार द्वारा बेटी बचाओए बेटी पढ़ाओए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाए सुकन्या समृद्धि योजनाए महिला शक्ति केंद्र योजना तथा महिला आरक्षण विधेयक जैसी पहलें लैंगिक समानता की दिशा में उल्लेखनीय कदम हैं। इन पहलों ने शिक्षाए स्वास्थ्य एवं आर्थिक भागीदारी में सुधार लाने का प्रयास किया हैए फिर भी उनके प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक मानसिकता में सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता बनी हुई है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि लैंगिक असमानता न केवल सामाजिक न्याय के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैए बल्कि भारत के सामाजिक. आर्थिक विकास एवं लोकतांत्रिक सुदृढ़ता को भी प्रभावित करती है। अतः संवैधानिक सुरक्षाए समावेशी नीतियाँए लैंगिक संवेदनशील प्रशासनिक ढाँचे तथा सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन ही वास्तविक लैंगिक समानता की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। |
|
| Keywords: | लैंगिक असमानताए, समकालीन भारत, महिला, सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, सतत विकास लक्ष्य, सार्वजनिक नीति, सरकारी पहल, संवैधानिक प्रावधान | |
| Certificate | ||
| Title: | स्त्रीवाद : मार्क्सवादोत्तर आणि वसाहतवादोत्तर अवलोकन | |
| Author(s) | प्रा. (डॉ.) संजय पंढरीनाथ गायकवाड | |
| Pages | 120-127 | DOI: 10.5281/zenodo.17227881 |
| Abstract: | स्त्रीवाद, मार्क्सवाद, नवमार्क्सवाद आणि पोस्टमार्क्सवाद यांचा अभ्यास हा सामाजिक-राजकीय बदल समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. स्त्रीवादाची मुळे प्राचीन काळात आढळतात, मात्र 18-19 व्या शतकात पश्चिम व भारतीय समाजात स्त्रियांच्या समान हक्कांसाठी ठोस चळवळी सुरू झाल्या. उदारमतवादी, समाजवादी, मूलगामी व उत्तर-आधुनिक अशा विविध प्रवाहांमधून स्त्रीवादाने समानतेचा पुरस्कार केला आहे. आंतरराष्ट्रीय विचारवंत मेरी ऑल्स्टोनक्राफ्ट, सिमोन द ब्युवोआर, बेट्टी फ्रीडन यांनी स्त्रीवादी विचारांना शास्त्रीय अधिष्ठान दिले, तर भारतात फुले, ब्राह्मो समाज यांचा ऐतिहासिक ठसा उमटला. स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण, रोजगार, समान वेतन, आरोग्य व राजकीय सहभागासाठी अनेक कायदे करण्यात आले तरीही ग्रामीण व मागास भागात असमानता टिकून आहे.
मार्क्सवादी स्त्रीवाद वर्ग, पितृसत्ता व भांडवलशाही यांमधील संबंधांचा पर्दाफाश करतो व सामाजिक क्रांतीला आवश्यक मानतो. महिलांच्या शिक्षणामुळे सामाजिक व आर्थिक स्वावलंबन साधले गेले. त्यानंतर विकसित झालेला नवमार्क्सवाद वर्ग संघर्षाबरोबर संस्कृती, विचारधारा, राज्यसत्ता यांचे विश्लेषण करतो. पोस्टमार्क्सवाद मात्र वर्गाच्या पलीकडे जात लिंग, जात, वंश, भाषा इत्यादी घटकांच्या अस्मिता व ओळखीवर आधारित बहुलवादी लोकशाहीची संकल्पना मांडतो. भारतीय संदर्भात जात, धर्म, लिंग या मुद्द्यांमुळे पोस्टमार्क्सवादाला नवीन सामाजिक व राजकीय संदर्भ देत अस्मिताधारित चळवळींना बळ मिळाले. अशा रीतीने स्त्रीवाद, मार्क्सवाद, नवमार्क्सवाद आणि पोस्टमार्क्सवाद यांद्वारे समाजातील विषमता व शोषणाला आव्हान देणारी वैचारिक परंपरा सतत विकसित होत गेली आहे. |
|
| Keywords: | स्त्रीवाद, मार्क्सवादोत्तर, वसाहतवादोत्तर, फेमिनिझम | |
| Certificate | ||
| Title: | भारतीय महिलायें और संवैद्यानिक अधिकार की जागरूकता | |
| Author(s) | ज्योति & डॉ. मयंक कुमार | |
| Pages | 128-132 | DOI: 10.5281/zenodo.17257932 |
| Abstract: | भारतीय मान्यताओं के अनुसार जहाॅ स्त्रीयों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं (मनुस्मृति) सृष्टि-सृजन और मानवीय सभ्यता के विकास में स्त्री व पुरूष दोनों की समान सृजनात्मक भूमिका रही है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी है। नारी अपने विविध रूपों में पुरूष का संवर्धन, प्रोत्साहन और शक्ति प्रदान करती है। माता के रूप में नारी पुरूष के चरित्र की संरोपण भूमि है। पत्नी के रूप में नारी पुरष उत्कर्ष का प्रसार स्तम्भ है। भिन्न-भिन्न देश, काल एवं परिस्थियों में महिलाओं की स्थिति, योगदान एवं स्वरूप को लेकर मतांतर रहे हैं।साहित्य एवं ज्ञान लोक ने नारी को गृह कार्य एवं काम प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है, तो काव्यकारों ने सौदर्य-बोधक रूवरूप में नारी निर्माण की ईसप्रक्रिया से समाज में महिलाओं की स्थिति असमानता, शोषण व उत्पीड़न के अनुभवों से जुडती चली गयी। उसे समाज में द्वितीय दर्जा दे दिया गया। वर्तमान समाज अर्थवाद का दास बनता जा रहा है। जहाॅ सम्पत्ति की अनियमिता से अधिक महत्व दिया जाता है। पूंजीवाद से सत्तावाद तथा सत्तावाद, सम्पत्ति, विलासितावाद, भेगवाद की ओर बढ़ रहा है। आदर्शत्मक मूल्यों का इस वर्तमान समाज में कोई महत्व नही है।
महिलाओं के अधिकारों के विभिन्न तरीके है जिसमें महिलाओं के साथ ही अबोध बालिकाएं भी सदियों से पुरूषों द्वारा अधिकारों के हनन की शिकार रही है तथा वर्तमान में भी इस स्थिति में ज्यादा सुधार नही हुआ है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय स्तरों पर महिलाओं की स्थिति को सुधार के लिए विशेष प्रावधान किए गये है। विश्व जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की कुला जनसंख्या की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। अर्थात् प्रारम्भ से ही विश्व में महिलायें समाज का एक अभिन्न अंग है परन्तु फिर भी महिलाओं की स्थिति भारत में ही नही अपितु विश्व के सभी देशों में प्रारम्भिक काल से ही दयनीय रही है। महिला विकास यात्रा संक्रमण से गुजर रही है जिसमें सकारात्मक तत्वों का समन्वय है इस शोध पत्र के अध्य्यन का उद्देश्य महिलाओं में सशक्तिकरण एवं जागरूकता लाना है साथ ही समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान पैदा करना है। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय नारी की स्थिति में काफी सुधारात्मक परिवर्तन हुये है। आजादी के 71 वर्षों के पश्चात् हम यदि कानूनी दृष्टिकोण से नारी के प्रति अपराधों को रोकने के लिए बनाये गये अधिनियमों की विवेचना करते है तो स्पष्ट परिलक्षित होता है की हमारे देश में नारी की गरिमामयी स्थिति को बनाये रखने के लिए काफी सारे कानून बनाये गये है, किन्तु पर्याप्त कानूनी शिक्षा के आभाव में कानून की जानकारी उनको नही मिल पाती। यहाॅ तक कि अधिकांश महिलाओं को यह ज्ञात नही होता कि उन्हें कौन-कौन से अधिकार प्राप्त है। प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं के उत्थान एवं उनके प्रति अपराधों को रोकने हेतु कौन-कौन से अधिकार है इसके बारे में वर्णन किया गया है। |
|
| Keywords: | भारतीय महिला, संविधान, अधिकार, जागरूकता | |
| Certificate | ||